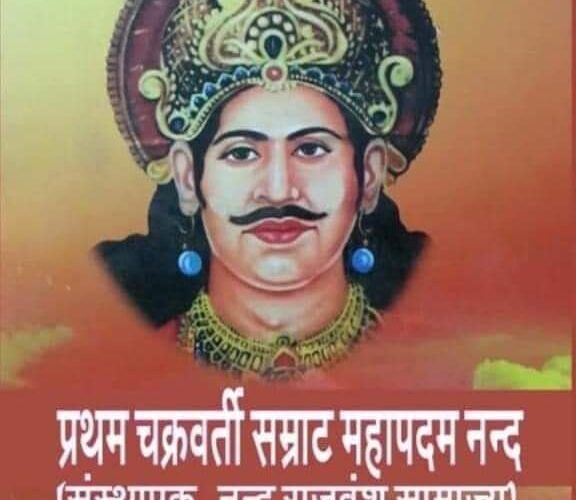नंदराजवंश का गौरवशाली इतिहास
प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे ऐतिहासिक महापुरुष किसी भगवान अथवा देवी देवता से किसी भी मामले में कम नही थे, उनकी नीति सम्पूर्ण विश्व में सराहनीय थी। जिसको देख सुन कर सारे विश्व के लोग भारत को विश्वगुरू, जगदगुरु तथा सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे और उनका लोहा भी मानते थे। मगर वह गौरवशाली प्राचीन इतिहास कहां गया एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज खोजने से भी नहीं मिलता है। डॉ राजवंश सहाय लिखते है कि ‘‘पतंजलि ने चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नन्द पर महानन्द नाम से एक महाकाव्य की रचना की थी जो समुद्रगुप्त द्वारा रचित ‘‘कृष्णचरित्र’’ के प्रथम तीन श्लोकों से ज्ञात होता है किन्तु इस महाकाव्य का विवरण मात्र ही आज शेष है।
ऐतिहासिक प्रमाण- चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनन्द का इतिहास, उड़ीसा में उदयगिरि पवर्तमाला से दक्षिणी भाग में एक प्राकृतिक गुफा है जिसे हाथीगुफा कहा जाता है उसमें प्राप्त पाली भाषा से मिलती–जुलती प्राकृत भाषा और ब्रहमी लिपि के १७ पंक्तियों में लिखे अभिलेख से प्राप्त होता है जिसके पंक्ति ६ और १२ में नन्दराज के बारे मे कलिंग के राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया माना जाता है। इस हाथी गुफा अभिलेख को ईसा पूर्व पहली सदी का माना गया है। इस अभिलेख के संबंध में के०पी० जायसवाल तथा बनर्जी के संयुक्त प्रयास विशेष विचारणीय हैं। दिनेश चन्द्र सरकार द्वारा जो पाठ प्रस्तुत किया गया है वह इस प्रकार है–
पुरातात्विक अभिलेखीय प्रमाण
१. भिंगारे (हि) त–रतन सपतेये सव–रठिक भोजके पादे वंदापयति (२) पंचमें च दनी वसे नंदराज –ति–वस –सतो (घा) टिंत तनसुलिय–वाटा–पणडिं नगरं पवेशयति सो–(अ) भिसितो च (छठे बस) राजसेयं संददंतो सबकर–बण ।’’
अनुवाद– जिनके छत्र भृगांर, हरित रत्न सम्पत्ति अपहृत कर लिये गये हैं उन राश्ट्रिक और भोजकों से व अपने चरणों की वन्दना कराते हैं। और पांचवे इस वर्ष तन सुलीय बाटा प्रणाली नहर को, जिसे नन्दराज ने ३०० वर्ष पूर्व खुदवाया था सहस्त्र मुद्रा व्यय करके नगर में प्रवेश करते हैं तथा राज्यभिषेक के छठें वर्ष राज्य के ऐश्वर्य के प्रदर्शन के निमित्त सभी राजकर माफ कर देते हैं।
२. ‘‘ मगधानं च विपुलं भयं जनेतो हथवं गंगाय पाययति (१) मगधं च राजनं बहसतिमितं पादे बंदापयति (१) नंदराजनीतं च कलिगं जिनं संनिकेश (पूजयति कोसात) गहरतन – पड़ी हारेहि अंग– मगध वसुं च नयति (२)
अनुवाद– मगधवासियों में विपुल भय उत्पन्न करते हुए हाथियों और घोड़ों को गंगा में पानी पिलाते हैं और मगध नरेश बहसतिमिति से अपने चरणों की वन्दना कराते हैं। और नन्द राज के नीति से कलिंग जीत की पूजा करते हैं। उस कोष से गृह रत्न अपहरण करके अंग और मगध का धन वसु से ले आते हैं।
अभिलेखीय पंक्तियों से मगध पति नन्दराज महापद्मनन्द एक ऐतिहासिक व राजनैतिक प्रथम चक्रवर्ती सम्राट तथा महापुरुष प्रकट होते हैं। इस अभिलेख से यह भी प्रमाणित होता है कि नन्दराज ने सिंचाई के लिये सहत्रों स्वर्ण मुद्रायें खर्च करके नहर खुदवाये थे और नन्दराज की नीति से कलिंग जीत की पूजा करते थे। शशिकान्त ने तिवस सतोंको महावीर संवत् का १०३ वर्ष अनुमान करते हैं जबकि मेरे समझ से वह ३०० वर्ष को प्रकट करता है जो खारवेल के प्रथम राज्यारोहण के तीन सौ वर्ष पूर्व नहर खुदवाये जाने को व्यक्त करता है। इस प्रकार खरवेल का समय ईसा पूर्व पहली शती निर्धारित होता है जिनके समकालीन शातकर्णि, यवनराज दमितीयस यानी बृहद्रथ पुत्र जरासंध और मगध राज बहसति मित्र यानि पुष्यमित्र शुंग राजा था।
इसी अभिलेख के पंक्ति १६ में पानतरिय – साथि वस सतेराज मुरिय काले पाठ के आधार पर इसे मौर्य काल के १६५ वे वर्ष का उल्लेख माना गया है तथा दिवस सत का अर्थ नन्दराज का ३०० वर्ष ग्रहण किया जाता है। इस अभिलेख से नन्द और मौर्य दोनों मगध के राजवंश प्रकट होते हैं जिसमें नन्दवंश मौर्य से पहले था या यह कहा जाय कि नन्दवंश के तुरन्त बाद ही मौर्यवंश मगध की गद्दी पर एक उत्त्ताराधिकार के रुप में आरुढ़ हुआ कोई अनुपयुक्त नही होगा किन्तु विद्वानों ने अभिलेख में जिसे मुरियकाल पढ़ा है वहाँ अभिलेख में वस्तुत: मुखिय कला लिखा हुआ है जिसका अर्थ मुख्य कला से है। इस प्रकार अभिलेख में मौर्य या मुरिय भाव का कहीं भी प्राप्त होना प्रमाणित नही है। इस प्रकार मौर्यवंश के द्वारा एक अलग राजवंश को व्यक्त करना सर्वथा अनुचित है।
आश्चर्य है कि सम्राट अशोक के अब तक के प्राप्त पुरातात्विक अभिलेख सबसे अधिक १६३ की संख्या में प्राप्त हुए हैं। किन्तु किसी भी अभिलेख में उनके वंश परम्परा को मौर्यवंशी नहीं कहा गया है। और न तो उनके द्वारा ही इस शब्द नाम को इंगित किया गया है। अत: इससे भी स्पष्ट होता है कि चन्द्रगुप्त अथवा सम्राट अशोक नन्दवंशी, नागवंशी मगधराज के परिवार के अभिन्न अंग हैं।
साहित्यिक प्रमाण :– अंगुत्तर निकाय में जिन सोलह महाजनपदों का वर्णन मिलता है वह कल्पना पर आधारित नही है। ये सोलह महाजनपद उस समय वस्तुत: मौजूद थे जो मगध पति, पृथ्वी पति, एकराट, एक छत्र राज्य करने वाले, सर्वक्षत्रांतक चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद द्वारा विजित किये गये थे तथा उन सब को अपने अधीन किये थे। भगवती सूत्र में सोलह महाजनपदों का उल्लेख है। ऐतिहासिक दृष्टि से बृहतकल्प, सूत्रभाष्य, कल्किपुराण, कथाकोष महत्वपूर्ण जैन ग्रन्थ हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पर्वन जिसकी रचना ईसा की बारहवीं शाताब्दी में हुई है, जिसमें स्पष्ट रूप से सम्राट महापद्म नन्द को गौरवशाली नाई, नापित जाति का बताया गया है। जिस जाति ने जैन–बौद्ध विचार धारा को आत्मसात करते हुए अपने परम्परागत शाल्य चिकित्सा, राजनैतिक व बौद्धाचार्य प्रवृत्ति से प्राचीन भारत को अन्धविश्वास से दूर करके विश्व पटल पर जगद्गुरू के रूप में स्थापित कर दिया। सच्चाई तो यह है कि इस जाति के जैसा दूसरा किसी जाति का इतिहास है ही नही जिसे गौरवशाली रक्त से विशुद्ध मूलनिवासी एवं प्राचीन कहा जा सके। पाणिनी के अष्टाध्यायी से हमें मौर्य काल से पूर्व भारत की राजनैतिक, सामाजिक व धार्मिक जानकारी मिलती है। साथ ही विशाखदत्त के मुद्राराक्षस, सोमदेव के कथा सारित्सागर और क्षेमेन्द्र की बृहतकथा मंजरी से मौर्य काल एवं उसके पूर्व की कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य के अर्थ शास्त्र के कुछ अध्याओं से चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नन्द के आदर्श शासन पद्धति का पता चलता है। विदेशी इतिहासकार कर्टियस ने भी नन्दराज महापद्म नन्द को नाई जाति का बताया है तथा सायरोपीडिया के अनुसार पश्चिमी एशिया के महान राष्ट्रों के बीच होने वाले संघर्ष में पंच बनने की कामना करने वाला सम्राट बहुत समृद्धवान एवं सैन्य शक्ति से मजबूत था।
क्या सम्राट महापद्म नन्द मगध के पूर्व राजवंश के उत्तराधिकारी थे?
पुराणों में शिशुनाग वंश के उपरान्त मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नन्द को बताया गया है। ऐतिहासिक विद्वानों के अनुसार शिशुनाग का नाम ब्रात्य नन्दी शिशुनाग था। डा० काशी प्रसाद जायसवाल के मत से ब्रात्य नन्दी शब्द उसके ब्रात्य क्षत्रिय होने का सूचक है। प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार ब्रात्य नंन्दी या क्षात्र बन्धु वह लोग थे जो मगध देश के पूरब में निवास करते थे तथा वैदिक संस्कृति को नही स्वीकार करते थे। उनके शिक्षा–दीक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा थी वे ब्राह्मणों के स्थान पर अर्हतों को पूज्य मानते थे तथा चैत्यों की आराधना करते थे।
मेरा मानना है कि मगध सम्राट ब्रात्य नन्दी शिशुनाग के नाम में ब्रात्य और नन्दी दोनों शब्द किसी न किसी रूप में नन्द राज, महापद्म नंन्द से जुड़ा हुआ है। ब्रात्य क्षत्रिय उसी को कहा गया है। जो राजा ब्राह्मणों को त्याग कर बौद्धिक बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे और शास्त्र धारण करने से ब्रात्य क्षत्रिय कहलाते थे। नन्दी शब्द नन्दराज या महापद्म शब्द नाम में जुड़े नन्द शब्द को ही उद्बोधित करता है। इस प्रकार नन्दराज महापद्म नन्द मगध के पूर्व शासक ब्रात्य नन्दी शिशुनाग का अभिन्न राजवंश प्रतीत होता है। ब्राह्मणी ग्रन्थों में सम्राट ब्रात्य नन्दी शिशुनाग को किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल का न बता कर शूद्र ही बताया गया है।
महाबोधिवंश सिंघल लेख में मगध सम्राट महापद्म नन्द को उग्रसेन भी कहा गया है। पुराणों तथा सिंघली दोनों में वंशावली लेखों में सम्राट नन्दिवर्धन के बाद महानन्दीन एवं महापद्म नन्द उग्रसेन को मगध का सम्राट बताया गया है। अत: दोनों वंशावली मगध सम्राटों को एक ही वंशावली बताते हैं जिससे इन्हें अलग राजवंश का व्यक्त करना सर्वथा अनुचित है।
उपरोक्त दोनों वंशावली में अधिकतर नामों में समरूपता प्राप्त होने के साथ नामों के क्रम में अंतर है किन्तु दोनों लेख प्रतापी सम्राट महापद्म नन्द की वंशावलीयों को एक बतलाते हैं। कारण कि दोनों वंशावलियों में क्रमश: महानन्दीन एवं महापद्म (उग्रसेन) के पिता के रूप में में नन्दि वर्धन के नाम उल्लेख हुआ है। महाबोधिवंश में जहां नन्दिवर्धन के पिता को काला शोक बताया गया है वहीं पुराणों में नन्दिवर्धन के पिता को उदयन कहा गया है। पुराणों का काकवर्ण ही महाबोधिवंश का कालाशोक है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में सम्राट महापद्मनन्द नन्दिवर्धन के पुत्र तथा काला शोक के पौत्र उजागर होते हैं।
सम्राट महापद्म नन्द जिन्हें नापित नाई कहा गया है बिना किसी विद्रोह के मगध के शासक बनते हैं और ३९ वर्षों तक एकक्षत्र राज करते हुए मगध को अखण्ड एवं समृद्धि भारत का दर्जा विश्व में प्रदान कराते हैं जो एक हत्या करके बने शासक द्वारा किया जाना कदापि सम्भव नही है। हत्या करके शासक बनने की कहानी आधुनिक इतिहासकारों द्वारा रची गई प्रतीत होती है। जबकि महापद्म नन्द वस्तविक उत्तराधिकारी कुल का नहीं मान कर ऊंच, ब्रात्य, क्षत्रिय एवं कुलीन राजा माना गया है। कुछ इतिहासकार महापद्म नन्द को शिशुनाग वंशी होने से उन्हें नाग क्षत्रिय एवं महानाग कहते हैं और नागों की उत्पत्ति महाभारत काल के ऋषि कश्यप की संतान बताते हैं जबकि महाभारत ग्रन्थ की रचना महापद्म नन्द के शासन काल से लगभग २०० वर्ष बाद हुई है। इसलिए उसके पूर्व के शासक उन लोगों की संतान वैâसे हो सकते हैं?
सिंहासनारोहण :– सम्राट महाद्म नन्द का मगध की गद्दी पर सिंहासनारोहण सम्राट कालाशोक या काकवर्ण की मृत्यु के ३१ वर्ष बाद यानी ३६४ ईशा पूर्व में हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद महापद्म की उपाधि नन्द ने अपने महान पराक्रम से छोटे-छोटे सभी राज्यों को मगध साम्राज्य में मिलाकर एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया तथा महापद्म की उपाधि २२ वर्ष, तारानाथ के अनुसार २९ वर्ष, जबकि यूनानी ग्रन्थ मैकिन्डल, इनवेजन ऑफ एलेक्जेन्डर में कहा गया है कि ३२६ ईसा पूर्व में जब चन्द्रगुप्त, सिकन्दर से भेंट किया था तब पाटलिपुत्र में नन्दराज का शासन चल रहा था। इस प्रकार नन्दराज का शासन अवधि ३६४ ईसा पूर्व से ३२६ ईसा पूर्व तक निर्धारित होता है। अर्थात नन्दराज महापद्म नन्द कुल ३९ वर्ष तक शासन किये।
विजयें व राजधानियां :– मगध सम्राट महापद्म नन्द जिन राज्यों पर विजय प्राप्त करके उन्हें मगध साम्राज्य में मिलाया था उनके नाम क्रमश: पुराणों एवं बौद्ध ग्रन्थों में पौरव, इच्छावाकु, पान्चाल, कौरव, हैहय, कलिंग, शूरसेन, मिथिला, अशमक, बीतिहोत्र, काशी, कटक प्रमुख राज्य थे। महापद्म नन्द ने समस्त उत्तरी भारत के समकालीन राजाओं को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। उसी तरह उसने कलिंग पर आक्रमण करके उसे भी अपने कब्जे में लिया था तथा नहर एवं बांध का निर्माण कराया था। डॉ० राय चौधरी के अनुसार दक्षिणा पथ का भाग भी नन्द साम्राज्य के अन्तर्गत था क्योंकि गोदावरी के तटपर ‘‘नव नन्द देहरा’’ नामक नगर को बसाये जाने का उल्लेख मिलता है। कृश्णा नदी की घाटी व मैसूर राज्य भी नन्द राज के विजित क्षेत्र थे और इन राज्यों के अलावा पहले से ही अंग, वत्स, अवंति, चंपा, लिच्छवी, वैशाली, कोशल राज्य सम्मिलित हो चुके थे। इस प्रकार महाद्म नन्द प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम सैन्य शक्ति से सर्व शक्तिमान विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे कोई ललकारने की हिम्मत नही कर सकता था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उत्तर में गंगा, यमुना के मैदान से लेकर दक्षिण में गोदावरी एवं कलिंग तक तथा पूरब में बंगाल से लेकर पंश्चिम में अफगानिस्तान तक का सम्पूर्ण भाग महापद्म नन्द के साम्राज्य में सम्मिलित था।
स्थाविराबलि चरित्र नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि नन्दराजा के मन्त्री कल्पक बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था, जो अपनी प्रवंचनाओं एवं कूटनीति से मगध साम्राज्य के विस्तार में काफी सहायता किया था। पुराणों के अनुसार नन्द राजा का नाम महापद्म अथवा महामद्मपति था जिसका अर्थ है असीम सेना अथवा अपार धन सम्पदा के स्वामी। जिस राजा के पास इतनी विशाल सेना हो वह अगर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी, कृश्णा, कावेरी की घाटी तक अथवा उसके समीपस्थ प्रदेशों का एकराट, एकक्षत्र होने का महत्वाकांक्षी हो तो इसमें कोई अत्युक्ति नही होगी। सिकन्दर के इतिहासकारों ने लिखा है कि व्यास नदी के पास बसने वाली जातियां सबसे शक्ति शाली थी और एक ही राजा के अधीन थीं जो सम्राट महापद्म नन्द के शक्ति एवं शासन को प्रमाणित करती हैं। पुराणों में लिखा है कि नन्दराज के शैशुनागों ने महिश्मती के पड़ोसी राज्य अवन्ती के शासकों को नीचा दिखाया था। प्राचीन भारत में जो शास्त्र धारण करके अपने क्षेत्र अथवा राज्य की रक्षा करते थे वे सभी राजा क्षत्रिय कहलाते थे चाहे वो किसी भी जाति अथवा वर्ण का क्यों न हो। उस समय तक जाति एवं वर्ण मात्र ब्राह्मणीय ग्रन्थकारों के ग्रन्थों तक सीमित था यानि व्यवहार में नही था और इसी प्रकार शुद्र शब्द का अर्थ भी सुचिता से था। पवित्र करने वाले के अर्थ में इसका प्रयोग होता था। इनकी उपस्थिति से प्रत्येक कार्य पवित्र होते थे, इसीलिए सम्राट महापद्म नन्द को शुद्र कहे जाने पर भी उनके द्वारा कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है और प्रतिवाद न करने का कारण यह भी है कि ये रचनायें महापद्म नन्द के शासनकाल से काफी बाद में की गई हैं।
सायरोपीडिया के अनुसार पश्चिमी एश्यिा में महान राष्ट्रों के बीच होने वाले संघर्ष में ‘‘सरपंच’’ बनने की भूमिका अदा करने वाला राजा बड़ा धनी प्रतापी था जो सम्राट महापद्म नन्द की प्रतिभा को उजागर करता है। भागवत पुराण के टीकाकार के अनुसार नन्दराज की दस पदम् सेना के कारण ही उनका नाम महापद्म पड़ा था। कर्टियस एवं डायडोरस के अनुसार उनकी सेना में बीस हजार घुड़सवार, तीन हजार हाथी की सेना, दो हजार रथ, तथा दो लाख की पैदल सेना थी। वहीं प्ल्ूटार्क के अनुसार अस्सी हजार अश्ववारोही, बहत्तर लाख की पैदल सेना, आठ हजार चार घोड़ों वाला रथ तथा छ: हजार हाथी की सेना थी। कथा सरित सागर में कहा गया है कि अयोध्या में महामद्म नन्द का सैन्य शिविर था तथा नन्दराज के पास ९९ करोड़ की स्वर्ण मुद्रायें थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार नन्दराज के पास सात प्रकार के बहुमूल्य जवाहरों की पांच निधियां थीं। इस प्रकार अनेकों श्रोंतों से प्रमाणित होता है कि सम्राट महापद्म नन्द के राज परिवार में अपार धन दौलत के ढेर थे तथा अपार सैन्य शक्ति से सम्पन्न थे जिसके बल पर उन्होंने महत्वपूर्ण विजय तथा मगध की साम्राज्य सीमा का विस्तार किया था।
नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं कि मैसूर के कई अभिलेखों के अनुसार महापद्म नन्द का वहां भी शासन होने की पुष्टि होती है। पुराणों में नन्दराज को ‘‘कलि’’ का अवतार तथा पृथ्वी का एकक्षत्र राजा व पृथ्वीपति बताया गया है। इस प्रकार इसमें संशय नही है कि चन्द्रगुप्त के समय में जो मगध की साम्राज्य की सीमा थी उसको नन्दराज के शासनकाल में ही मगध साम्राज्य की सीमा के अधीन कर लिया गया था। यहाँ तक की नन्दराज का केंद्रीय शासन पद्धति जिसे एरियन ने नन्द साम्राज्य में उत्कृष्ट आन्तरिक शासन का होना बताया है। नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि बड़े ही आश्चर्य की बात है कि सम्राट महापद्म नन्द जैसे महान योद्धा एवं अखण्ड भारत को एक सूत्र में बांध कर एकक्षत्र राज्य करने वाले प्रतापी सम्राट को मात्र शुद्रों का राजपरिवार जानकर उनके बारे में कुछ लिखा ही नही गया, मगर यहीं कोई सवर्ण राजा होता तो उसकी प्रशंसा में एक और रामायण या महाभारत की रचना अवश्य हो गई होती। बी०ए० स्मिथ ने महापद्म नन्द की रचनाओं में किये गये परिवर्तन के बारे में कहा है कि नन्दराज ब्राह्मणों के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध थे इसी कारण से उनके राज्य काल को बारहवीं सदी के कवि चन्द ने एतिहासिक काल क्रम से निकाल दिया तथा उनके द्वारा चलाये विक्रम संवत जिसने ‘‘आनन्द’’ विनान्द का प्रयोग बन्द किया था, जिससे नन्द काल के ऐतिहासिक ९० वर्ष निकाल दिये गये। स्पष्ट है कि जिन मूलनिवासी आर्य (शुद्र) राजाओं, राजवंशो को ब्राह्मणी षड़यंत्रों द्वारा इतिहास से मिटाया जा सकता है उससे सम्बन्धित लेखों पर अवश्य ही लीपापोती की गई होगी। इस विषय पर मैकडानिल लिखते हैं कि सर्वाधिक पुरानी रचना ऋग्वेद को ३००० साल तक बिना परिवर्तन किये सम्भाल कर रखी गई जबकि उसके बाद की रचनाओं में यानी नन्द काल से जितनी रचनाओं को लिपि बद्ध किया गया उसमें इतना परिवर्तन हुआ कि उन्हें आज अपनी पूर्ण मूल अवस्था में लाना असम्भव है। किन्तु लीपा-पोती करने वाले को यह पता नही था कि यथार्थ को कितना भी दबाया एवं छिपाया जाय एक न एक दिन आवश्य ही अपने वास्तविक रूप में उजागर हो जाता है। महाबोधिवंश के अनुसार बिम्बसार के सातवें उत्तराधिकारी के रूप में शिशुनाग तथा दसवें उत्तराधिकारी के रूप में महापद्मनन्द (उग्रसेन) हुए जो मगध के महान सम्राट प्रमाणित हुए।
शासन प्रबन्ध :– नन्दराज महापद्मनन्द एक कुशल योद्धा, महान विजेता ही नहीं वरन् योग्य शासक भी थे जो इतने बड़े साम्राज्य की शासन व्यवस्था को शान्ति पूर्वक ३९ वर्षों तक शान से चलाये। चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था नन्दराज द्वारा विकसित शासन प्रबन्ध था। नन्दराज के शासन तन्त्र का उद्देश्य लोकहित था जहां एक ओर आर्थिक विकास और राज्य की समृद्धि के अनेक ठोस कदम उठाये गये, शिल्पियों व व्यापारियों के जान-माल की सुरक्षा की गयी वहीं दूसरी ओर जनता को उनकी अनुचित तथा शोषणात्मक कार्य विधियों से बचाने के लिये कठोर नियम भी बनाये गये थे। अनाथ मृत सैनिकों तथा राज्य कर्मचारियों के भरण–पोषण का भार राज्य के ऊपर था। नन्दराज ने अपने शासन व्यवस्था में सत्ता का केन्द्रीय करण, उचित न्याय व्यवस्था, नगर शासन, कृर्षि शिल्प उद्योग, वाणिज्य एवं व्यापार के लिए अनेकों कारगर उपाय किये थे। यह भी पता चलता है कि अतिरिक्त आय को पूरा करने के उददेश्य से कृर्षि का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने स्वयं उस भूमि में खेती कराई जहां पहले खेती नहीं होती थी। उसने सिंचाई के साधनों में वृद्धि की और यातायात के साधनों का विकास करके व्यापार की उन्नति की सरकार ने सिक्कों का प्रचलन बढ़ाकर व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया साथ ही उद्योगों और व्यापार पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था और इन तथ्यों को कदापि भुलाया नही जा सकता है।
नन्द साम्राज्य दूर-दूर तक विस्तृत था, नन्द वंश के संस्थापक का उद्देश्य एकात्मक राज्य स्थापित करना था। क्षत्रपों पर महान विजय प्राप्त कर विशाल साम्राज्य को स्थापित कर के एकक्षत्र जैसे पदों के प्रयोग का और कुछ अर्थ नही हो सकता। एरियन ने व्यास नदी के पार आन्तरिक शासन की उत्कृष्ट व्यवस्था का उल्लेख किया है जिसमें अभिजात तंन्त्र प्रचलित था और यह अभिजात वर्ग अपने अधिकारों का प्रयोग न्यायोचित और संयमित ढंग से करता था। नन्द राज ने अपने साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को गंगा के डेल्टा तथा अवध के आगे क्षेत्रों के लोगों को मगध क्षेत्र में पर्याप्त शासनाधिकार दे रखा था। किन्तु गृह प्रदेश को जिसमें मगध (दक्षिणी बिहार) बृज्जि (उत्तर बिहार) काशी (वाराणसी) कोशल (अवध) आदि जनपद शामिल थे। प्रशासन व्यवस्था लगभग वैसी ही थी जैसी कि दिल्ली के सुल्तानों की दिल्ली सूबे में थी और दोआब के प्रदेशों में थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार के बज्जि देश की राजधानी वैशाली में भी राजा की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। अयोध्या में एक सैनिक शिविर का भी प्रसंग मिलता है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के यूनानी पर्ववेक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है कि नन्दराज के शासनकाल में नोमार्क (जिलाधीश) और हाई पार्क (क्षत्रप) जैसे अधिकारी भी हुआ करते थे।
मुद्रा/सिक्के– नन्दकालीन सिक्के को आहत मुद्रा अथवा ढले सिक्के कहा जाता है इसका निर्माण भारतीय टकसालियों द्वारा किया गया था। नन्दकाल में सोना अन्य देशों के अपेक्षाकृत भारत में सस्ता था जिससे यहाँ के सोने के सिक्के जो विदेशों में चले गये वे फिर वहीं रह गये क्योंकि सोना वहाँ मंहगा था। सम्राट नन्दराज महापदमनन्द की टकसाल में सोने चांदी का अनुपात १:१३:३ रखा गया था। जान मार्सल महोदय को तक्षशिला में भिड़ढूह की खुदाई में मिट्टी के कलश में ११६७ आहत मुद्राएं मिली थीं। उन आहत मुद्राओं का वजन ३२ रत्ती अथवा लगभग ५८ ग्रेन है। उसी वजन का एक अद्वितीय सिक्का भी मिला है जो अब बर्लिन के म्यूजियम में है। उसकी शक्ल के आधार पर पर्सीगार्डनर ने उस सिक्के का सम्बन्ध भारत से बताया है। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनी की अष्टाध्यायी एवं उसके भाष्य पर दृष्टि रखते हुए छोटे-छोटे चिन्हों से उदटं्कित मुद्राओं को आहत मुद्रा नाम दिया है। डा० पाठक इस पंचमार्क्ड सिक्कों को टंकित मुद्रा कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं।
आहत मुद्राओं की प्राप्ति सर्वप्रथम १८वीं शताब्दी में कर्नल कोण्डबेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से प्राप्त हुई थी। आज आहत मुद्राओं की सैकड़ों निधियां पचासों जगहों से प्राप्त हुई है। डा० परमेश्वरी लाल गुप्त ने ३० हजार से अधिक आहत मुद्राओं का परीक्षण किया है। गोरखपुर परिक्षेत्र से भौलानाथ चतुर्वेदी को स्वर्ण की दो आहत मुद्राओं की प्राप्ति हुई थी इन आहत मुद्राओं के पुराभाग पर क्रमश: सात व आठ की संख्या में चिन्ह विद्यमान है। जिसका प्रकाशन जे०एन०एस० आई० वाल्यूम ३४ में हुआ है।
डा० राजवंत राव के अनुसार यदि स्वर्ण मुद्राओं का उल्लेख प्राचीन साहित्यों में है तो इसकी वास्तविक स्थिती भी अवश्य रही है। विनय पिटक में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्रावस्ती के सेठ अनाथ पिण्डक ने स्वर्ण मुद्राओं को विछाकर श्रावस्ती के राजकुमार जेत कुमार के जेतबन को भगवान बुद्ध के लिए क्रय किया था। अनाथपिण्डक द्वारा स्वर्ण मुद्राओं के विछाए जाने का वर्णन द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की कलाकृतियों में भी हुआ है। इससे प्रकट होता है कि स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन नन्दराज महापद्मनन्द के शासनकाल से पहले ही हो चुका था मगर प्रसिद्ध पुरातत्वविद् विजय कुमार ठाकुर के अनुसार भारत में दूसरी बार शहरीकरण का क्रम ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में अर्थात ३६४ ई०पू० में शुरू हुआ जो बिना किसी रूकावट के गुप्त काल (५५० ईसवी) तक चला इतना ही नहीं यही भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल था जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ इसी काल में प्रथम बार लेखन कला का पुस्तकें लिखने के लिए प्रयोग हुआ देश का महत्वपूर्ण साहित्यक कोश बौद्ध जैन व सनातन धर्म के धार्मिक ग्रन्थों व संस्कृत के व्याकरण व नाटकों की रचना भी इसी काल में हुई। पत्थर व पक्की ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण कला के लिए हुआ। पत्थर की सुन्दरतम् मूर्तियां गढ़ी गईं। मूर्तिकला में गान्धार कला इसी युग की देन है देश में पहली बार सोने, चांदी व ताबें के सिक्कों का प्रचलन हुआ देश में शिल्पिक (औद्योगिक) श्रेणियों का जाल विछा देशी तथा विदशी व्यापार में भरपूर प्रगति की, परिणामस्वरूप शहरी तथा ग्रामीण दोनो क्षेत्रों का जीवन स्तर समृद्ध और सुखमय हो गया था। जिसका वर्णन अर्बनाइजेशन इन ऐंसेन्ट इन्डिया पृष्ट १० में विजय कुमार ठाकुर ने किया इन्होने पृष्ठ ५६ में लिखा है कि अर्हत उपाली जो नाई का बेटा था। बौद्धभिक्षु तथा महान विद्वान बन गया जिसने विनय पिटक की रचना की जो बौद्ध धर्म की शीर्षस्थ रचना मानी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि नन्दराज महापद्मनन्द का शासनकाल सिक्का प्रचलन से लेकर विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय रहा है।
परमेश्वरी लाल गुप्त ने भीर टीले की निधि को नन्दकाल की मुद्राएं स्वीकार की हैं इस काल को डा० गुप्त ने ३६४ से ३२० ई० पू० तक माना है इस निधि से सिकन्दर और फिलिप्स की मुद्राएं नई अवस्था में प्राप्त हुई हैं। रैप्सन के अनुसार इन दोनों वर्गों के सिक्कों को एथेन्स के सिक्कों की नकल पर भारत में बनाया हुआ बताया हैं। जेम्स फेरुगेशन के अनुसार नन्दकालीन सिक्कों पर नागों के नाम और नाग चिन्ह मुख्य रूप से पाया गया है जो नन्दराज के नागटोटिम को अपनाए जाने की ओर इंगित करता है। उत्खनन में सिक्के बनाने वाले सांचे एवं टक्साल भी प्राप्त हुए है।
शिक्षा व्यवस्था– नन्दकाल में शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त ही उच्चकोटि की थी शिक्षक आदरणीय एवं पुज्य थे उस समय सबके लिए शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था। निआर्क्स एवं मेगास्थनीज के अनुसार अक्सर सभी लोग पढ़ना एंव लिखना जानते थे विद्यालयों में शिल्पिक शिक्षाएं अनिवार्य रूप में दी जाती थी साथ ही सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था।जिससे मगध साम्राज्य शिक्षा के मामले में समृद्ध होकर एक सैन्य राष्ष्ट्र के रूप में दृष्टिगोचर होता है वृहदकथा के अनुसार पाणिनी और वररूचि नन्दराज महामदमनन्द के मित्र थे आर्यमंजुश्री मूलकल्प में पाणीनी को नन्दराज का मित्र बताया गया है। राज शेखर के अनुसार पाटलिपुत्र में एक विद्वान सभा थी जहाँ वर्श, उपवर्श, पाणिनी, पिंगल, व्याड़ि, वररूचि, और कात्यायन आदि थे। जहाँ शास्त्रीय ज्ञान की परीक्षा होती थी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नन्दराज विद्वानों की प्रतियोगिता के लिए
शास्त्रार्थों को कराने में रूचि लेते थे।
बौद्ध परम्परा के अनुसार तक्षशिला से चाणक्य शास्त्रार्थ के लिए पाटलिपुत्र गया था। जिससे प्रमाणित होता है कि नंदराज के शासनकाल मे तक्षशिला, पाटलिपुत्र एवं नालन्दा में विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था। ऐसे विद्धानों को पाकर के नन्दराज ने विश्वविद्यालयों की स्थापना कराया था। उपरोक्त विद्वान ही उनके दरबार के नवरत्न थे। जिससे पाटलिपुत्र ही नहीं अपितु सम्पुर्ण मगध साम्राज्य विद्या एवं लक्ष्मी (धन-सम्पदा) से परिपूर्ण होकर समृद्धशाली बन गया था। तथा विश्व में जगत गुरु के नाम से पुकारा जाने लगा था। कहा जाता है कि नन्दराज ने इन विश्वविद्यालयों की व्यवस्था के लिए सौ-सौ गांव दे दिये थे जिनके प्राप्त आय से प्रत्येक विश्वविद्यालय के ३००० विद्यार्थियों तथा सैकड़ों आचार्यों का खर्च चलता था। नन्दमौर्य काल में शिक्षा केन्द्रों की खर्च व्यवस्था के लिए छात्र स्वयं कपड़ा भी बुना करते थे।
नन्दकाल में नापित जाति की सामाजिक–आर्थिक स्थिति–छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारतीय समाज में ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र वर्ण व्यवस्था थी जो परिवर्तनीय थी किन्तु अपरिवर्तनीय जाति व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था चाहने वाले लोगों के या तो दिमाग में थी या तो उनके पोथियों तक सीमित थी जातियों का विस्तार एवं प्रसार १८४ ईसा पूर्व के बाद हुयी मगर इन जाति व्यवस्था कारों, द्वारा जिन लोगों को नापित कहा गया है वह सामाजिक धार्मिक, आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अत्यन्त ही उच्च एवं पूज्यनीय लोग थे, जो पूरोहिती के सम्पूर्ण कार्यों को कराने के साथ-साथ सेना नायक एवं राजसिंहासन तक के पदों पर विराजमान होते थे।
भगवान गौतम बुद्ध के प्रथम महान शिष्य अरहत विनयधर उपाली को अंगुतर निकाय में नापित (नाई) कहा गया है जो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धम्म संघ के प्रथम उत्तराधिकारी हुए जिन्हें नालंदा शब्द सागर में (लॉ मैन) न्यायी पुरुष कहा गया है तथा जो पालि ग्रन्थों के रचनाकार हैं। उनकी प्रेरणा से ही मगध के सम्राटों से लेकर सम्पूर्ण भारतवासी तक बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए और इनके वंशज बौद्धाचार्य भन्ते, अरहत, राजा के मंत्री, पुरोहित, शिक्षक एवं शासक (राजा) तक अपने सेवा और शील व्यवहार के माध्यम से बनने लगे जिससे नापित जाति की सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक स्तर ऊँचा हो गया। लोग उस समय दान-दक्षिणा किसी ब्राहमण को न देकर नापित बौद्धाचार्य को ही दिया करते थे जो उनका मुण्डन करके प्रव्रज्जित आदि करते थे। मज्झिम निकाय २/४/३ में कहा गया है कि भगवान बुद्ध एक बार मुखादेव के आम्रवन में विहार कर रहे थे उसी आम्रवन में एक जगह पर भगवान मुस्करा उठे। भगवान बुद्ध का मुस्कुराना देखकर आयुष्मान आनन्द सोचने लगे कि तथागत बिना कारण मुस्कुराते नहीं, अवश्य ही कोई राज है। तब आनन्द ने चीवर को एक कन्धे पर करके जिधर भगवान थे उधर हाथ जोड़ कर बोले भन्ते, भगवान के मुस्कुराने का क्या कारण है? भगवान बोले आनन्द पूर्व काल में इसी मिथिला में मुखदेव नामक एक धार्मिक राजा थे जो अपने सिर के पके बाल देखकर अपने ज्येष्ठ पुत्र कुमार को बुलाकर कहा–बेटा मेरे देवदूत प्रकट हो गये सिर में पके बाल दिखाई दे रहे हैं। मैंने मनुष्य काम भोग लिए अब दिव्य भोगों के खोजने का समय है आओ बेटा बेटे इस राज्य को प्राप्त करो मैं केशमुड़ा कर कसाय वस्त्र पहन कर घर से बेघर हो प्रव्रज्जित होऊँगा। जब तुम भी अपने सिर में पके बाल देखना तब नापित को दान में एक–दो गाँव देकर प्रव्रज्जित हो लेना और मुखादेव ने नापित को बुलाकर इसी जगह पर प्रव्रज्जित हो कर दो गाँव दान स्वरूप दिया मुखादेव ने अपने बेटे कुमार से यह भी कहा कि बेटा तुम मेरे अंतिम पुरुष मत बनना अर्थात तुम भी अपने बेटों को इसी तरह की शिक्षा देकर दिव्य जीवन की प्राप्ति का कार्य कराना। उपरोक्त प्रसंग से ज्ञात होता है कि नापित जाति, कुलवंश का सामाजिक स्तर उस काल में अत्यन्त ही उच्च था जो बुद्धवादी हुआ करते थे। जन साधारण से लेकर राजा, महाराजा तक नापित से मुंडन करा कर विनय एवं शील की शिक्षा लेकर दान दक्षिणा देते थे जिससे नापित जाति के लोग चल अचल सम्पत्ति से परिपूर्ण हो कर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर राजा एवं महाराजा तक की उपाधि प्राप्त करते थे।
उदान अट्टकथा में कहा गया है कि भगवान बुद्ध ज्ञानप्राप्ति के बाद जब कपिल वस्तु गए तो सर्वप्रथम कपिलपुर के नन्द कुमार एवं नन्द राजा को प्रव्रज्जित किये जो नन्द नापित को प्रस्तुत करता है उसके बाद कोपिया के आम्रवन में छ: शाक्य कुमारों के पूर्व नापित नन्द कुमार उपाली को भगवान बुद्ध द्वारा प्रव्रज्जित किया गया है जिसका वर्णन चुल्ल्बग में किया गया है अरहत उपाली का सम्बन्ध जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी से भी था जैन ग्रन्थों में इनके बारे में अनेक स्थलों पर वर्णन मिलता है आश्चर्य है कि जैन ग्रन्थों में महाबीर स्वामी के भाई को नन्दवर्धन बताया गया है जिन्हें पुराणों एवं सिंहल के लेखों में महानन्द अथवा महापदमनन्द का पिता कहा गया है वैशाली के आठों गणसंघ मगध साम्राज्य के अभिन्न अंग थे तथा राजगृह के बाद वैशाली भी मगध की राजधानी बनी थी इससे प्रकट होता है कि महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का ही दूसरा नाम काकवर्ण था जिन्हों ने बाद में राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया तथा उनके पुत्रों को नापित कहा गया। आचार्य चतुरसेन शास्त्री वैशाली की नगर वधू में नापित गुरू के विषय में जो प्रसंग प्रस्तुत करते हैं उससे यह प्रकट होता है कि नापित जाति के लोग उस समय सम्राट या राज दरबार से परस्पर जुड़े हुए थे। वह लिखते हैं कि – राजगृह के चौराहे पर एक खरकुटी थी खरकुटी छोटी सी थी पर वह राजगृह (मगधपुर) भर में प्रसिद्ध थी उसके स्वामी का नाम प्रभंजन था। उससे सभी बाल मुड़वाते थे वह बड़ा बाचाल, चतुर और बहुज्ञ था उसकी पहुँच छोटे से लेकर बड़े तक सर्वत्र थी वह बड़ा आनन्दी प्रकृति का जीव था लोग उससे प्रेम करते, उसकी बातों से प्रसन्न होते तथा उससे डरते भी थे डरने का कारण यह था कि लोग कानो-कान उसके विषय में बहुधा कहते थे कि सम्राट और वर्शकार भी उसे बहुत मानते हैं और वह प्रसाद, महालय अर्थात किला में जाकर भी उनके बाल मूड़ता है कुछ लोगों का कहना था कि इसे सम्राट और वर्शकार के अनेकों गुप्त भेद मालूम हैं इससे सम्राट तथा महामात्य (महामंत्री) भी भय खाते हैं परन्तु जब–जब कोई उससे इन महामान्य जनों की चर्चा करता है तब वह मुस्कुरा कर टाल जाता है वह बहुधा धार्मिक कथा प्रसंग लोगों को सुनाया करता है। लोग उसे नापित गुरु कहकर पुकारते थे।
दो दण्ड रात्रि व्यतीत हो चुकी थी किन्तु खरकुटी में अब भी ग्राहकों की काफी भीड़–भाड़ थी प्रभंजन अपने दो सहायको के साथ काम में जुटा था। एक युवक आया और नौकरी की याचना किया जो एक ब्रात्य (बुद्धवादी सेनानी) था उसको लेकर प्रभंजन खरकुटी के भीतर एक छोटे से प्रांगण में ले गया, प्रांगण के उस पार कई छोटी-छोटी कोठरियां थी एक को खोलकर उसने कहा आयुश अभी तुम यहां विश्राम करो एक मुहुर्त में मैं काम से निपट कर तुम्हारे आहार की व्यवस्था कर दूँगा। आज मैं बहुत व्यस्त रहा मित्र तुमने सुना सम्राट ने आर्य आमात्य को पद से हटा दिया है? प्रभंजन तेजी से यह बात कहकर लौट रहा था कि आगन्तुक व्यक्ति ने अपना उश्णीय एक ओर फेक दिया और वापस लौटते हुए नापित गुरु से कहा प्रभंजन। अतर्कित और अकल्पित ढंग पर नाम सुनकर वह चौंक पड़ा उसने लौट कर देखा तो साक्षात मगध महामात्य (महामंत्री) वहाँ उपस्थित थे नापित गुरू ने प्रणाम किया महामात्य ने कहा प्रभंजन लेख की सामग्री लाओ और अभी एक लम्बी यात्रा की तैयारी करो। प्रभंजन की वाचालता लुप्त हो गयी वह तेजी से दूसरी कोठरी में गया और लेख की सामग्री उसने महामात्य के सामने रख दी।
प्रभंजन ने कहा– आर्य यदि एक घड़ी भर का मुझे अवकाश दें ……… हाँ हा इतना काल तो मुझे लेख में लग जायेगा। परन्तु प्रभंजन तेरी यह यात्रा अत्यन्त गुप्त होगी और मैं अभी तीन दिन इसी वेश में इस खरकुटी में रहुँगा ऐसा यत्न करो कि इसका किसी को ज्ञान न हो, ऐसा ही होगा– आर्य (मुलनिवासी उच्चलोगों के सम्मान की उपाधि) महामात्य लेखलिखने लगे। प्रभंजन ने जाकर झट-पट ग्राहकों से छुट्टी ले कर सहयोगियों को आवश्यक आदेंश दिए फिर एक तलवार वस्त्रों में छिपाया, छद्मवेश धारण किया और पर्यटक बंजारे के भेष में महामात्य के सम्मुख उपस्थित हुआ महामात्य ने देखा और मुस्कुराकर समर्थन किया फिर एक मुहरबंद पत्र और मुहरो से भरी एक थैली देकर कहा यह पत्र जितना शीघ्र सम्भव हो श्रावस्ती के सेना पति उदायी को अथवा उनके सहकारी को मिल जाए और कुछ कहना भी होगा आर्य– नहीं। यहाँ से यों ही जाना होगा प्रभंजन। मार्ग में एक अश्व खरीद लेना किन्तु वह भी साधारण ही हो जिससे तुम दस्युओं की दृष्टि में न आ सको। हाँ श्रावस्ती से लौट कर तुम वैशाली के मार्ग में मेरी प्रतीक्षा करना जाओ प्रभंजन। प्रभंजन ने अभिवादन किया और तेजी से अंधकार में विलीन हो गया। अमात्य कोठरी का द्वार बन्द कर दीपक सामने रख कर लेख लिखने में व्यस्त हो गए किसी को भी नहीं प्रतीत हुआ कि इस नापित गुरू की खरकुटी के एक कोठरी में बैठे महामहिम मगध महामात्य नीति चक्र चला रहे हैं इस प्रकार प्रकट होता है कि नापित लोग उस काल में अमात्य महामात्य अथवा सम्राट व बौद्धचार्य अर्हत आदि महापुरुषों से सीधे जुड़े हुए थे जिन्हें प्राचीन ग्रन्थों में राजन्य अर्थात राजा का भाई कहा गया हैं। ऐसे में उनका रक्तमय सम्बंध था। और ये राजनीति के प्रत्येक गुप्त से गुप्त कार्य को जानते तथा करते रहते थे। स्वतंत्र भारत के बाद भी बड़े घरानों से इनके पारस्परिक सम्बंध दिखाई देता है नापित वंश के लोग भारतीय समाज का एक गौरवमयी अभिन्न अंग है जिसे आज ब्राहमण अपने साथ में लेकर उनके गौरव को भुना रहे है तथा उन्हें उनका वास्तविक हिस्सा भी नहीं देते जो कि एक चिन्तनीय विषय है।
नन्दराज महापद्म नन्द की मृत्यु:– एरियन के अनुसार सिकन्दर की सेना जब रावी नदी के तट पर ३२६ ईसा पूर्व में पहुंची थी तब पाटलिपुत्र में नन्दराज महापद्मनन्द का शासन था। उक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि नन्दराज की मृत्यु ३२६ ईसा पूर्व के अन्त में या ३२५ ईसा पूर्व के प्रथम माह में हुई थी।
नन्दराज महापद्मनन्द ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे जिसके बारे में हमने ही बता दिया है। इनके ब्राह्मण विरोधी नीति से ब्राह्मणों के सामने आजीविका की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। उनकी भू-सुर एवं उच्च बनने की रणनीति तथा उनके द्वारा चलाये जा रहे यज्ञ, अनुष्ठान लगभग बन्द हो चुके थे, उनको भी लकड़ी काट कर बेंचने, कृर्षि करने रथ बनाने, सन्देश वाहक का कार्य करने, कसाईगीरी आदि का काम करके जीवीकोपार्जन करना पड़ता था। उनको न तो कोई दान दक्षिणा देने वाला था और न तो कोई बड़ा उच्च मानने वाला। उनको मजबूर होकर राज्यादेश का पालन करना पड़त्ाा था। जबकि ब्राह्मण दरिद्र रहकर भी उच्च कहलाना चाहते थे और यह नन्दराज महाद्म नन्द के रहते सम्भव नहीं था।
चाणक्य तक्षशिला से जब पहली बार पाटलिपुत्र आया तो उसने नन्दराज की पारिवारिक स्थिति को मालूम किया। चाणक्य द्वारा चन्द्रगुप्त को सम्राट बनने के लिए उत्तेजित किया। चन्द्रगुप्त चाणक्य के कुटिल नीति को समझ नही सका और वह चाणक्य को अपना हितैषी समझकर उसको पाटलिपुत्र में स्थान दिला दिया। यहाँ तक कि चन्द्रगुप्त ने एक दिन नन्दराज से अपने युवराज बनने का प्रस्ताव भी रख दिया। फिर उसकी माता मुरा देवी द्वारा भी अपने पुत्र को युवराज बनाये जाने का प्रस्ताव नन्दराज महापद्मनन्द के समक्ष रखा। जिसको सुनकर नन्दराज ने कहा– उसे युवा सेनापति बना देता हूँ, उम्र हो जाने पर उसे युवराज या सम्राट भी बना देंगे। इसके बाद चन्द्रगुप्त मगध की विशालतम सेना का युवा सेनापति नियुक्त हो गया। चन्द्रगुप्त अन्य भाइयों से भी दूरी बना कर रहने लगा। अन्य सभी भाई उससे उम्र में श्रेष्ठ थे तथा कोई विदिशा का प्रशासक था तो कोई उत्तरापथ, नन्दीवर्धन कलिंग, कटक, अयोध्या, मथुरा, व काश्मीर के शासक थे घनानन्द मगध साम्राज्य के युवराज थे। बाकी नन्दराज के शासन व्यवस्था में प्रशासक बनकर सहयोग करते थे।
सिकन्दर नामक यूनानी आक्रमणकारी के मगध की सीमा की ओर पहुँचने की बात सुनकर अपने युवराज घनानन्द को तथा सभी राजाओं को सेना सहित मगध की पश्चिमोत्तर सीमा तक पहुँचने की घोषणा नन्दराज द्वारा की गई। नन्दराज की सैन्य शक्ति एवं प्रताप के बारे में सुनकर सिकन्दर की सेना में विद्रोह हो जाता है और सभी स्वदेश यूनान लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मगध सीमा में प्रवेश करने का मतलब है मौत के मुंह में प्रवेश करना। यह बात सुनकर सिकन्दर का भी हौसला पस्त हो गया और अन्तत: सेना को स्वदेश लौटने का आदेश दे दिया। उसी बीच चन्द्रगुप्त अकेले सिकन्दर से जाकर मिलता है और कहता है कि सिकन्दर तुम मगध पर आक्रमण करो तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, मै तुम्हारा साथ दूंगा। सिकन्दर चन्द्रगुप्त को डांट कर भगा देता है और सभी यूनान के लिए प्रस्थान कर देते हैं। चन्द्रगुप्त यह सोच कर गया था कि यदि सिकन्दर और नन्दराज में युद्ध होता है तो सिकन्दर के विजयी होने पर मैं स्थानीय होने के नाते मगध का महाक्षत्रप बन जाऊंगा, फिर मैं उनको दरकिनार करके मगध का सम्राट बन जाऊंगा, किन्तु नन्दराज के शौर्य बल से ही सिकन्दर के हिम्मत का दिवाला निकल गया और चन्द्रगुप्त की सोच केवल सोच बनकर रह गई।
सिकन्दर के सेनाओं की यूनान वापसी की खबर सुनकर पाटलिपुत्र में खुशियों का माहौल बन गया था। चाणक्य उर्फ कौटिल्य भी उस खुशी के माहौल में उपस्थित हुआ और नन्दराज महापद्म नन्द की प्रशंसा गाथा गाने लगा कि आप सचमुख बड़े महान हैं कि आपको पाटलिपुत्र छोड़कर जाना तक नही पड़ा और विश्व विजयी का स्वप्न देखकर भारत आने वाला सिकन्दर आपकी राज्य सीमा से कोसों दूर पहले से ही वापस लौट गया। उसी समय चाणक्य ने अपने कुटी पर सपरिवार भोज निमंत्रण का प्रस्ताव भी रख दिया जिसको सुनकर नन्दराज ने स्वीकार कर लिया।
चाणक्य ने कुटी पर निश्चित तिथि को नन्दराज द्वारा सपरिवार भोजन करने की जानकारी होने के बाद चाणक्य नन्दराज के रसोईदार सकटार और सुलक्षणा से सम्पर्क साधने लगा। निश्चित तिथि को नन्दराज महामद्मनन्द के दोनों रसोईयेदार चाणक्य की कुटी पर पहुँच गये तथा विषयुक्त स्वादिष्ट भोजन बना दिये यह जानकर कि चन्द्रगुप्त भी इस प्रयोजन में सम्मिलित है। निश्चित समय पर नन्दराज सपरिवार चाणक्य की कुटी पर पहुँच गये। भोजन करने के पूर्व ही सूचना मिलती है कि पूरब दिशा में कहीं कुछ बवाल हो गया है जिसको सुनकर कुछ सेनाओ को लेकर घनानन्द उधर चले जाते है बाकी लोग चाणक्य की कुटी पर भोजन करने लगते है और विषयुक्त भोजन करने से एक के बाद एक एक की मौत हो जाती है। मौत की खबर सुनकर चाणक्य, चन्द्रगुप्त एवं दोनों रसोइये मगध छोड़कर रातों–रात उत्तरापथ की ओर भाग जाते हैं तथा सेल्यूकश की शरण में चले जाते हैं। घनानन्द जब चाणक्य की कुटिया पर आता है तो सबको विषयुक्त खाने से मरा हुआ पाता है उसको समझने में देरी नही होती है वह तुरन्त चाणक्य एवं रसोइयेदार को खोजता है किन्तु किसी का अता-पता नहीं चलता है। जब चन्द्रगुप्त को भी नही पाता है तो वह समझ गया कि यह गहरी साजिश के तहत कार्य हुआ है। और अन्तत: घनानन्द मगध का सम्राट बनकर ३२६ई.पू. में मगध की गद्दी पर बैठा। विषयुक्त भोजन से नन्दराज की मृत्यु का वर्णन जहाँ मुद्राराक्षस में मिलता है वहीं जस्टिन के लेखो से चन्द्रगुप्त एवं चाणक्य को उत्तरापथ में सेल्यूकश के यहां रहने का वर्णन भी प्राप्त होता है। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इसी कुटिल नीति से चाणक्य नन्द वंश में फूट डालकर नन्दराज के साम्राज्य का विनाश किया।
नन्दराज के नवनन्द एवं उत्तराधिकारी :– नन्दराज के नवनन्द जो क्रमश: विभिन्न राजधानियों के माध्यम से शासन किये–
१. पन्डुक, सहल्य अथवा सहलिन (बंगाल का सेनवंश) :– नन्दराज महापद्मनन्द के ज्येष्ठ पुत्र पन्डुक जिनको पुराणों में सहल्य अथव्ाा सहलिन कहा गया है, नन्दराज के शासनकाल में उत्तर बिहार में स्थित वैशाली के कुमार थे तथा उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशज मगध सम्राज्य के प्रशासक के रूप में रहकर शासन करते रहे, प्रतीत होता है इनके वंशज आगे चलकर पूरब दक्षिण की ओर बंगाल चले गये हों और अपने पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनन्द (उग्रसेन) के नाम पर सेन नामांत धारण कर शासन करने लगे हों और उसी कुल से बंगाल के आदि सूर्या राजा बीरसेन हुए। जो मथुरा सुकेत, क्योन्थल, एवं मण्डी के सेन वंश के जनक बन गये जो ३३० ईसा पूर्व से १२९० ईसवी तक शासन किये।
२. सुकल्प अथवा पन्डुगति (अयोध्या का देववंश) :– नन्दराज के द्वितीय पुत्र को महाबोधि वंश में पन्डुगति तथा पुराणों में सुकल्प कहा गया है। कथा सरित्सागर के अनुसार अयोध्या में नन्दराज का सैन्य शिविर था जहां सुकल्प एक कुशल प्रशासक एवं सेना नायक के रूप में रहकर उसकी व्यवस्था देखते थे तथा कोशल को अवध राज्य बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई होगी। अवध राज्य यानी वह राज्य जहां किसी भी प्रकार की हिंसा या बलि पूजा नही होती हो जबकी इसके पूर्व यहां पूजा में पशु बलि अनिवार्य होने का विवरण प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है जिसको पूर्णतया समाप्त कराया और यही कारण है कि उन्हें सुकल्प तक कहा गया है यानी अच्छा रहने योग्य स्थान बनाने वाला। इन्ही के उत्तराधिकारी १८५ ईसापूर्व के बाद मूलदेव, वायुदेव, धनदेव, के रूप में हुये जिनके सिक्के अलमोड़ा के पास से प्राप्त हुए हैं।
३. भूतपाल अथवा भूतनन्दी विदिशा का नन्दी वंश) :– चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नन्द के तृतीय पुत्र भूतपाल अथवा भूत नन्दी विदिशा के कुमार अथवा प्रशासक थे नन्दराज के शासनकाल में उनके पश्चिम दक्षिण के राज्यों के शासन प्रबन्ध को देखते थे। नन्दराज का यह वंशज अपने नाम के साथ नन्द अथवा नन्दी लगाना ज्यादा उपयुक्त समझा। विदिशा के ये शासक कलान्तर में पद्मावती एवं मथुरा के भी शासक रहे तथा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किये। इतिहासकारों ने भूतपाल अथवा भूतनन्दी के शासन के काल को १५० वर्ष पूर्व से मानते हैं किन्तु मेरा विचार है कि भूतपाल का विदिशा में शासन ३४० ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था।
४. राष्ट्रपाल (महाराष्ट्र का सातवाहन कलिंग का मेघ वाहन वंश) :– महाबोधि वंश अनुसार नन्दराज के चौथेपुत्र राष्ट्रपाल थे। राष्ट्रपाल के कुशल प्रशासक एवं प्रतापी होने से इस राज्य का नाम राष्ट्रपाल के नाम पर महाराष्ट्र कहा जाने लगा। ये गोदावरी नदी के उत्तर तट पर पैठन अथवा प्रतिष्ठान नामक नगर को अपनी राजधानी बनाये थे। राष्ट्रपाल द्वारा ही मैसूर के क्षेत्र, अशमक राज्य एवं महाराष्ट्र के राज्यों की देखभाल प्रशासक के रूप में की जाती थी जिसकी केन्द्रीय व्यवस्था नन्दराज महापद्मनन्द के हाथों में रहती थी। प्रतीत होता है इनके पुत्र ही नन्दराज के मृत्यु के बाद आन्ध्र भृत्य कहे गये, क्योंकि ये केन्द्रीय शासन व्यवस्था में एक मात्र एक प्रशासक (जनसेवक) के रूप में नियुक्त होते थे। इसीलिये ब्राह्मणी ग्रन्थों, पुराणों में यह आन्ध भृत्य कहे गये। राष्ट्रपाल के पुत्र ही सातवाहन एवं मेघवाहन थे जो बाद में पूर्वी घाट उड़ीसा क्षेत्र पश्चिमी घाट महाराष्ट्र क्षेत्र के अलग-अलग शासक बन गये।
५. गोविशाणक (उत्तराखण्ड, गोविशाण का कुलिन्द वंश) :– महाबोधिवंश के अनुसार मगध के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट नन्दराज महापद्मनन्द के पाचवें पुत्र गोविशाणक थे। नन्दराज ने उत्तरापथ में विजय अर्जित किया था रैप्सन महोदय का विचार है कि नन्दवंश के संस्थापक का सम्बन्ध गोविशाण के कुनिन्द राजवंश से था जो नन्द भी कहलाते थे। नन्दराज के गोविशाण विजय के समय नन्दराज के पुत्र गोविशाणक का जन्म हुआ हो या गोविशाणक को वहाँ का प्रशासक बनाये जाने पर उस राजधानी का नाम गोविशाण रखा गया हो। सम्भव यहीं लगता है कि नन्दराज द्वारा गोविशाणक को प्रशासक बनाते समय एक नये नगर को बसाया गया हो और वहां उनके लिए किला बनवाया गया हो जिसका नामकरण गोविशाण नगर रखा हो। नइके उत्तराधिकारी क्रमश: विशवदेव, धनमूर्ति, बृहतपाल, बलमूर्ति अमोधमूर्ति, विश्वशिवदत्त, हरीदत्त, शिवपाल, क्षतेशवर, भानुरावण हुए जो लगभग २३२ ईसापूर्व से २९० ईसवी तक शासन किया।
६. दस सिद्धक :– मगध साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नन्द (उग्रसेन) के छठवें पुत्र दस सिद्धक थे। नन्दराज की एक राजधानी मध्य क्षेत्र के लिए वाकाटक में थी जहाँ नन्दराज के छठवें पुत्र दस सिद्धक ने अपनी राजधानी बनाया किन्तु इनके पितामह नन्दिवर्धन के नाम पर नन्दराज द्वारा बसाये गये सुन्दर नगर नन्दिवर्धन नगर को भी इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में प्रयुक्त किया जो आज नागपुर के नाम से जाना जाता है। दस सिद्धक ने ही सर्वप्रथम विन्ध्य क्षेत्र में अपने शक्ति का सर्म्वधन किया इसलिए इन्हें विन्ध्य शक्ति भी कहा गया जिन्होंने २५० ईसा पूर्व से ५१० ईसवी तक शासन किये।
७. कैवर्त– नन्दराज महापद्म नन्द का सातवां पुत्र वैâवर्त था। जिसका वर्णन महाबोधि वंश में किया गया है। यह एक महान सेनानायक तथा कुशल प्रशासक थे। नन्दराज के अन्य पुत्रों की तरह वैâवर्त किसी राजधानी के प्रशासक न होकर बल्कि अपने पिता के केन्द्रीय प्रशासन के मुख्य संचालक थे तथा सम्राट महापद्म नन्द (उग्रसेन) जहां कहीं भी जाते थे मुख्य अंगरक्षक के रूप में उनके साथ–साथ रहते थे। प्रथम पत्नी से उत्पन्न दोनों छोटे पुत्र केवर्त और घनानन्द तथा दूसरी पत्नी मुरा से उत्पन्न चन्द्र नन्द अथवा चन्द्रगुप्त ये तीनों पुत्र नन्दराज के पास पाटलिपुत्र की राजधानी में रहकर उनके कार्यों में सहयोग करते थे जिसमें चन्द्रगुप्त सबसे छोटा व कम उम्र का था। वैâवर्त की मृत्यु नन्दराज के साथ ही विषयुक्त भोजन करने से हो गई जिससे इनका कोई राजवंश आगे नही चल सका।
८. सम्राट घनानन्द :– घनानन्द सम्राट महापद्म नन्द की प्रथम पत्नी महानन्दिनी से उत्पन्न अन्तिम पुत्र था। यह जब युवराज था तब इसने अनेकों शक्तिशाली राज्यों को मगध साम्राज्य के अधीन करा दिया। नन्दराज की मृत्यु के बाद ३२६ ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना। नन्दराज एवं भाई वैâवर्त की मृत्यु के बाद यह बहादुर योद्धा शोक ग्रस्त रहने लगा फिर भी इसकी बहादुरी की चर्चा से कोई भी इसके सम्राज्य की तरफ आक्रमण करने की हिम्मत नही कर सका। घनानन्द भी पिता महापद्म नन्द की तरह वैदिक कर्मकाण्ड एवं हिंसामयी यज्ञ के सख्त विरोधी थे। सिकन्दर के सेनापति सैल्यूकस की सैनिक मद्द से इनका सौतेला भाई चन्द्रगुप्त ३२२ ईसा पूर्व में मगध की सत्ता प्राप्त करने के लिए चढ़ाई किया, जिससे युद्ध के दौरान घनानन्द की मृत्यु हो गई और मगध की सत्ता चन्द्रगुप्त को प्राप्त हुई।
९. चन्द्रनन्द या चन्द्रगुप्त :– महामद्मनन्द की मुरा नाम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को ही चन्द्रनन्द अथवा चन्द्रगुप्त कहा गया है। जिसे मौर्य वंश का संस्थापक कहा गया है। मुद्राराक्षस में चन्द्रगुप्त को नन्द की संतान तथा वायु पुराण में चन्द्रगुप्त को नंदवंशीय राजा कहा गया है। आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक अनार्थ राजकुमार राजा की शूद्र पत्नी (दारजी) से उत्पन्न बतलाया गया है भले ही राजा स्वयं मूल निवासी क्यों न रहा हो। महापद्मननद का जन्म भी शुद्र पत्नी से बताया गया है जबकि नन्दिवर्धन, कालाशोक, शिशुनाग, अजात शत्रु विम्बिसार, आदि स्वयं मूल निवासी अनार्य शासक थे। ऐसी ही बात चन्द्रगुप्त के बारे में भी कही गई हैं कि वह नन्दराज की मुरा नाम की शुद्र पत्नी से उत्पन्न हुआ था। ठीक ऐसी ही बात अशोक के बारे में भी कही गई है कि वह बिन्दुसार की नाईन पत्नी पटरानी धर्मादेवी से उत्पन्न हुआ था। कहा जा सकता है कि मगध के सारे राजा मूल निवासी, अनार्य, शुद्र एवं नाई थे जो मोर भी पाला करते थे अथवा मोर पालकों से संबन्धित थे।
मोर मौर्य परिवार का शाही चिन्ह था। टौटिज्म के इस विचार का समर्थन बौद्ध तथा जैन धर्म के ग्रन्थों से भी होता है। अत: यह बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाती है कि मौर्य परिवार निश्चित ही देशी अनार्य, शुद्रों का परिवार था जो नापित (नाई) जाति से संम्बन्धित था। जो वैâम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया के न्न्दत्त् झ्. १९९ एम. आर. गोयल के.ए. हिस्ट्री ऑफ इम्पीरियल गुप्ता के पृष्ठ ७५ पर एवं बी.ए. स्मिथ के पुस्तक ‘‘नन्द डायनेस्टी ऑफ मगध –अशोक के पृष्ठ ३ पर वर्णित है उक्त उद्धरण सिन्धु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता शुद्र एवं वणिक के पृष्ठ ११२ पर भी देख सकते हैं।’’
चन्द्रगुप्त का आकर्षक मेगस्थनीज के लेखों से प्राप्त होता है जो अब उद्धरणों के रूप में प्राप्त होते है। चन्द्रगुप्त २४ वर्ष तक कुशल शासन करने के उपरान्त २९८ ईसापूर्व में मगध की सत्ता अपने पुत्र बिन्दुसार को सौंप कर भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चले गये और वहीं समाधिलीन हो गये। चन्द्रगुप्त घनानन्द के बाद ३२२ ई० पू० में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ तथा २४ वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। इसके बाद इनका पुत्र बिन्दुसार जिसे अमित्रघात भी कहा जाता हैं, मगध पर शासन किया।
बिन्दुसार :– जैन परम्पराओं के अनुसार बिन्दुसार चन्द्रगुप्त की दुर्धरा नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था। बिन्दुसार राजमहल के आनन्दों में पलने के बावजूद वह फौलादी जिस्म का व्यक्ति था। इसने साम्राज्य के अन्तर्गत सारे अमित्रों (शत्रुओं) का विनाश करके ‘‘अमित्रघात’’ की उपाधि धारण की थी। बिन्दुसार के मंत्री सुवन्धु ने चाणक्य नामक अमित्र की हत्या की थी। अमित्रों की वर्ण व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त कर दिया था। बिन्दुसार ने दक्षिण भारत के चोल, पान्डुव, राज्य को मगध सम्राज्य में मिलाया था।
‘‘अशोकावदानमाला’’ एवं महावंश टीका में धम्मा अथवा महादेवी को पटरानी बताया गया है। जिससे दो पुत्र अशोक एवं विगत शोक, (तिश्य) उत्पन्न हुये थे। धम्मा को वहीं नाईन भी बताया गया है सुभद्रांगीं से सुमन अथवा सुशीम का जन्म हुआ। जो अशोक से उम्र में बड़ा था। किन्तु अशोक की तरह सुशीम सम्राट के योग्य नही था। बिन्दुसार के समय में मेगास्थनीज की जगह डायमेच्स राजदूत बनकर आया था। उस समय मिस्र, यूनान आदि देशों से अच्छे सम्बन्ध थे। २६ वर्ष शासन करने के बाद बिन्दुसार की मृत्यु २७२ ईसा पूर्व में हो गई।
सुमन (सुशीम) :–बिन्दुसार की मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र सुशीम मगध के गद्दी पर आसीन हुए। सुशीम के व्यवहार से मगध के मंत्री खुश नही थे वे सभी अशोक को सम्राट बनाना चाहते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बिन्दुसार की मृत्यु के समय अशोक की आयु २१ वर्ष की थी। जबकी २५ वर्ष से पूर्व सम्राट पद के लिए राज्याभिषेक की परिपाटी नहीं थीं। इसलिए चार वर्ष तक सुशीम ने मगध की सत्ता को सम्भाला था। उसके बाद २६९ ईसा पूर्व में अशोक मगध सम्राज्य के सम्राट बने।
सम्राट अशोक महान :– प्राचीन ग्रन्थों एवं अभिलेखों में अशोक को देवानांप्रिय, प्रियदर्शी एवं दशरथ नाम से सम्बोधित किया गया है। अशोक का जन्म बिन्दुसार की नाईन पत्नी धम्मा देवी से हुआ था। अशोक एक महान विजेता था। उसके पूर्वजों ने जिस प्रदेश को हस्तगत करने में असफलता प्राप्त की अशोक प्रथम प्रयास में उस पर पूर्ण विजय प्राप्त की। उनकी प्रथम एवं अन्तिम विजय कलिंग विजय थी। उसके बाद उसने शास्त्र युद्ध का परित्याग कर दिया तथा धम्म विजय की ओर अग्रसर हुआ। डॉ० स्मिथ के शब्दों में – ‘‘यदि अशोक योग्य न होता तो वह अपने विशाल साम्राज्य पर ४० वर्षो तक शान्ति पूर्वक सफल शासन नहीं कर सका होता, और अपना ऐसा नाम न छोड़ गया होता– जिसे लोग २००० वर्षों के उपरान्त भी नही भूल सके हैं’’ सम्राट अशोक २२९ ईसा पूर्व तक शासन किये।
सम्राट अशोक के १४ शिलालेख, ६ स्तम्भ लेख, ६ लघु लेख, ३गुहा लेख, पाशाण कलक लेख, लघु स्तम्भ लेख तथा विदेशी भाषाओं के लेख सहित कुल १६३ लेख प्राप्त हुए हैं। इतना अन्य किसी भी सम्राट के प्राचीन लेख प्राप्त नही हुये हैं किन्त आश्चर्य है कि उनके किसी भी लेख में अपने आप को मौर्य वंशी नही कहा गया है। गया के निकट नागार्जुनी पहाड़ी पर तीन गुफाओं पर दशरथ नाम लिखा हुआ है। जिसका पत्थर पालिस अशोक काल के निर्मित बताती हैं जो आजीविकों (श्रमणों) को दान दी गई थी। बुद्ध विश्व विजय में निर्गुणानन्द महाथेरो जी सम्राट अशोक को ही दशरथ मानते हैं उनका कहना है कि– सम्राट अशोक की तीन रानियाँ थीं। देवी, पद्मावती और असन्धिमित्रा। इसमें असन्धिमित्रा मगध साम्राज्य की पटरानी थी। अशोक के चार पुत्र एवं दो पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। जिसमें देवी से महेन्द्र और संघमित्रा, पद्मावती से कुणाल, असन्धिमित्रा से चारूमती का जन्म हुआ था। असन्धिमित्रा के असमय मृत्यु हो जाने पर अशोक तिश्यरक्षिता (वैâकेई) नामक पत्नी को लाये और पटरानी बनाये जिससे दो पुत्र जालौक एवं कुस्तान हुये थे।
दिव्यावदान के अनुसार तिश्यरक्षिता कुणाल से प्रेम करने लगी। कुणाल उसे मां तुल्य समझता था उससे प्रेम का प्रतिदान न पाकर तिश्यरक्षिता उसपर कुपित हो गई और उसकी दोनों आंखे एवं कुमार के पद से च्युत करने का आदेश भेज दी। उस समय सम्राट रूग्णावस्था में थे। सम्राट का आदेश मानकर कुणाल ने उसका अक्षरश: पालन किया। वधिक बुलाकर अपनी दोनों आंखें निकलवा दिया तथा प्रशासक का पद त्याग कर अपनी पत्नी बच्चे सहित वन गमन हो गये। कुणाल को ही बौद्ध जातक कथाओं में राम कहा गया है। इनके राज्य निर्वासन की कथा पर ही वाल्मीकि ने राम बनवास की कथा बनाई थी रामायण की रचना भी घटना के लगभग १०० वर्ष बाद हुई जिसमें पूर्व घटनाओं को आधार बनाया गया है।
पुराणों में अशोक के उत्तराधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं :–
(१) कुणाल–८ वर्ष (२) बन्धुपालित (पुत्र–१) ८ वर्ष (३) इन्द्रपालित, दयाद (बन्धुपालित का भाई) १० वर्ष (४) दशौन, नप्ता (बन्धुपालित का पौत्र) ७वर्ष (५) दशरथ (दशौन का पुत्र) ८ वर्ष (६) सम्प्रति (दशरथ का पुत्र) ६ वर्ष (७) शालिसुक –१३ वर्ष (८) देवधर्मन –७ वर्ष (९) सतधनुश–(देवधर्मन का पुत्र) ८ वर्ष (१०) वृहद्रथ–७ वर्ष।
पुराणों में वर्णित उपरोक्त उत्तराधिकारियों में कुणाल एवं बृहद्रथ ही इतिहासकारों द्वारा सर्वमान्य हैं इनमें कुणाल को ८ वर्ष शासन करते हुए बताया गया है जबकि ये ८ वर्ष प्रशासक के रूप में कार्य किये। कुणाल के अंधा हो को जाने पर सम्राट अशोक ने अपने पौत्र बृहद्रथ को २२९ ई०पू० में मगध की राजगद्दी पर बैठाया।
पुराणों के वर्णित नामों में केवल दशरथ के बारे में ही पूरा लिपिक प्रमाण उपलब्ध है। परन्तु बौद्ध और जैन विवरणों में उनका नाम नही आता है। सम्पदि अथवा सम्प्रति का नाम बौद्ध और जैन साहित्यों में प्रख्यात है। दिव्यावदान के अनुसार सम्पदि अथवा संम्प्रति कुणाल का पुत्र था। मगध सम्राज्य के सिंहासन पर उनकों मंत्रियों ने विचित्र स्थिति में स्थापित किया था। अशोक ने बौद्ध संघ को एक सौ करोड़ के दान की प्रतिज्ञा की थी। अपने शासनकाल में वह केवल ९६ करोड़ दे पाया था। शेष चार करोड़ के बदले उसने अपना राज्य ही संघ को समर्पित कर दिया। मंत्रियों ने प्रयत्न करके ये चार करोड़ रुपये इकठ्ठे कर लिए। संघ को वह धन देकर राज्य को बंधक से छुड़ा लिया और संप्रति को सिंहासन पर बैठा दिया। जैन विवरणों के अनुसार संप्रति ही अशोक का उत्तराधिकारी था। कारण कि कुणाल अन्धे हो चुक थे, महेन्द्र और संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बन गये थे तथा तिश्यरक्षिता के गलत व्यवहार से जालौक एवं कुस्तान उत्तराधिकार से वंचित कर दिये गये थे।इससे स्पष्ट होता है कि अशोक के बाद मगध की सत्ता संप्रति, सम्पदि अथवा वृहद्रथ ने ही उत्तराधिकारी के रूप में सम्भाला था।
श्री एच. जी. वेल्स के अनुसार– अशोक का नाम बड़े-बड़े और विभिन्न उपाधियों वाले सहस्त्रों शासकों में, जिनका वर्णन इतिहास में आता है, तारे की तरह चमकता है। बोल्गा से जापान तक आज भी उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत अशोक के सिद्धान्तों का परित्याग भले ही कर चुके हों, किन्तु उसके परम्परागत महत्व को सुरक्षित रखे हुए हैं। कान्सटेनटाइन और चार्लमेन से भी कहीं बढ़कर लोग अशोक के स्मृति का आदर करते हैं।
प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० रमेश मजूमदार के शब्दों में ‘‘अशोक का साम्राज्य विस्तृत होते हुए भी शास्त्र की इकाई के रूप में संगठित था। एक ही राज्यादेश पेशावर से बंगाल तक और कश्मीर से मैसूर तक चलता था।
कुणाल :– पुराणों में कुणाल को आठ वर्ष शासन करते हुये बताया गया है जबकि दिव्यावदान के अनुसार कुणाल ने राज्य नही किया। क्योंकि वे अन्धे हो चुके थे। कुणाल का विवाह कंचनमाला नामक रूपवती कन्या से हुआ था। जिससे सम्प्रति, अथवा वृहद्रथ का जन्म हुआ था।
कुणाल के अन्धा हो जाने के बाद सम्राट अशोक ने अपने पौत्र बृहद्रथ को मगध सम्राट बनाया। यदि कुणाल का शासन पुराणों के अनुसार मान लिया जाय तो २२१ ईसा पूर्व तक कुणाल मगध के प्रशासक थे इसके बाद बृहद्रथ शासक थे।
बृहद्रथ (सम्प्रति/सम्पदि) :– बृहद्रथ एक वीर योद्धा तथा कट्टर बौद्धिक शासक थे। अपने शासनकाल में हिन्सामयी सारे यज्ञों को बन्द कर दिये थे। जिससे यज्ञ के नाम पर मान्स खाने वालों के सामने समस्या उत्पन्न हो गयी थी। इनके दरबार में चीन का एक निवासी पुश्यमित्र शुंग आया और सेवक बनने की याचना किया। उसे सेना में सिपाही के रूप में रख लिया गया, फिर वह अपने कला कौशल से सेनापति का पद प्राप्त कर लिया। पुश्यमित्र शुंग पतजंलि से ब्राह्मणी धर्म की दीक्षा लेकर अपने आपको कट्टर ब्राह्मण बनाने लगा।
सेनापति बनने के बाद उसकी निगाहें सम्राट बनने में लगी रहीं। एक दिन सेना के निरीक्षण के दौरान १८५ ई० पू० में पुश्यमित्र शुंग नामक सेनापति ने सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दिया और मगध का सम्राट बन बैठा।
बाणभट्ट के हर्षचरित्र के अनुसार कपटी सेनापति पुश्यमित्र ने यह बहाना करके कि महाराज को समस्त सेना का निरीक्षण कराया जायेगा। निरीक्षण के दौरान हत्या कर दिया। इस प्रकार महाराजा बृहद्रथ २२१ ईसा पूर्व से १८५ ईसा पूर्व तक कुल ३६ वर्ष मगध साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट रहे।
विष्णु पुराण में कथन है कि सेनापति पुश्यमित्र शुंग सम्राट बृहद्रथ को र्निमूल कर २६ वर्षों तक शासन करेगा जबकि सम्राट बृहद्रथ के हत्या के समय उनका पुत्र जरासंघ राजगृह का राजा था। उस समय जब इस घटना की जानकारी हुई तब वह अपने पिता के हत्यारे पुश्यमित्र शुंग एवं उसके सहयोगियों से बदला लेने के लिए बहुत बड़ा युद्ध छेड़ दिया जिसे बाद में महाभारत युद्ध का नाम दिया गया। उसने समकालीन वैश्णवधर्मी सभी राजाओं को राजगृह में वैâद कर लिया था जिन सभी को एक साथ नरबलि किये जाने का वर्णन महाभारत ग्रन्थ में मिलता है। यहाँ तक कि उस ग्रन्थ में शाक्तिशाली राजा बासुदेव कृष्ण को मथुरा के किला से द्वारिकापुरी भगाने वाले जरासंघ का वर्णन महाभारत में मिलता है। जरासंघ के रहते सम्राट बृहद्रथ कावंश र्निमूल हो जायेगा, कहा जाना सरासर गलत है जबकि उसी महाभारत ग्रन्थ एवं पूराणों में जरासंघ के पिता का नाम स्पष्ट रूप में सम्राट बृहद्रथ बताया गया है।
महाभारत में जरासंघ के पुत्र सहदेव का वर्णन है उसी ग्रन्थ में सहदेव के भाई को भीम बताया है। भीम के पुत्र को घटोत्कच कहा गया है। जो हिडम्बा से उत्पन्न हुये थे इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि सहदेव/भीम के पुत्र घटोत्चक जो महाभारत के महाबली शक्तिशाली योद्धा थे। ये सभी ऐतिहासिक पुरुष थे। इतिहास में घटोत्कक्ष के पुत्र को चन्द्रगुप्त प्रथम कहा गया है और चन्द्रगुप्त प्रथम के साथ–साथ सभी गुप्त नामान्तधारी राजाओं को गुप्तवंशीय राजा कहा गया है। महाराज घटोत्कच को भी गुप्तवंशीय राजा कहा गया। यहाँ तक कि घटोत्चक के पिता सहदेव/श्री गुप्त को गुप्तवंश का संस्थापक कहा गया है। जो राजवंश ५७० ई० तक प्राचीन भारत में शासक रहा। ऐसी राजवंश परम्परा को निर्मूल हो जायेगा, भविष्यवाणी के माध्यम से कहा जाना प्रपंच नहीं तो और क्या हो सकता है? उनका यह भी कथन गलत है कि पुश्यमित्र शुंग २६ वर्षों तक शासन करेगा। कारण कि सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुश्यमित्र शुंग १ वर्ष भी पाटलिपुत्र में चैन से जरासंघ के रहते शासन नहीं कर सका। उसके अश्वमेद्य यज्ञ के घोड़े को रोकने वाला, उसके यज्ञ अनुश्ठान को नष्ट करने वाला तथा मथुरा एवं साकेत के किले को अपने अधिकार में लेते हुए पाटिलपुत्र तक पहुॅचने वाला दमित्रियस कोई और नहीं जरासंध ही था जो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेने के लिए यवन रूप धारण किया था। जिसका वर्णन गार्गी संहिता में मिलता है।
जरासंध के डर से पुश्यमित्रशुंग अपनी राजधानी पाटिलपुत्र से हटाकर अयोध्या में बनाया। मगर वहाँ भी जरासंध, मूलदेव के रूप में भेष बदलकर अयोध्या के किला में घुसकर पुश्यमित्र शुंग एवं उसके पुत्र सुमित्र को मार डाला। जिसका वर्णन मालविकाग्निमित्रम में किया गया है। इस प्रकार पुश्यमित्र शुंग ६ वर्ष से अधिक शासन नहीं कर सका। उसके शासन अवधि को लम्बा बताने के प्रयास में ब्राम्हणी ग्रन्थों ६वर्ष के शासन अवधि को २६ वर्ष के रूप में दर्शाया गया है।
आश्चर्य के साथ कहना पड़ता है कि ब्राहम्णवादी लिखने एवं प्रपंच गढ़ने में इतना माहिर थे कि जिस पुश्यमित्रशुंग को अयोध्या का राम तथा बृहद्रथ को लंका का रावण घोिषत करके रामायण की रचना कराये और उसे त्रेता युग की घटना बताये, वही लोग सम्राट बृहद्रथ के पुत्र जरासंघ एवं उनके पौत्र घटोंत्कच एवं दामाद कंस आदि को द्वापर युग का राजा बता दिये तथा उनके लिये एक अलग ग्रन्थ महाभारत की रचना कर दिये। जबकि ऐतिहासिक दृष्टि से रामायण का रचनाकाल अथवा त्रेतायुग १८५ ईसा पूर्व से १७९ ई० पूर्व तक, तथा १७९ ई० पूर्व से ७६ ईसवीं तक महाभारत का काल था। जिस काल में जरासंध, सहदेव, को कृष्णा अपने कुटनीतिक चाल में मिलाकर जरासंध का वध कर दिया और मगध की गद्दी पर सहदेव का राज्यभिषेक हुआ जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है। इस ऐतिहासिक तथ्य कि वास्तविकता यह है कि पुश्यमित्र शुंग के शासन काल में रामायण की सर्व प्रथम रचना महर्षि बाल्मिकि द्वारा की गई। उसी समय पंतजलि ने सर्वप्रथम कौरव पांडव युद्ध नामक एक छोटी सी कथा की रचना की गई जिस कथा का विस्तार ३८० ई ० के बाद चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में महर्षि वेदव्यास ने किया जिसका नाम महाभारत ग्रन्थ पड़ा। जिसे अब व्यवस्थावादी उसे द्वापर युग की घटना बताते है।
महर्षि पतंजलि प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती नापित सम्राट महापद्मनन्द के गौरवशाली ऐतिहासिक चरित्र के ऊपर ‘‘महानन्द’’ नामक एवं व्यापक महाकाव्य की रचना किये थे जिसका वर्णन समुद्रगुप्त द्वारा रचित कृष्णचरित के प्रथम तीन श्लोको से व्यक्त हुआ है किन्तु वह महानन्द नामक महाकाव्य मूल रूप में अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उक्त महाकाव्य को व्यवस्थावादियों द्वारा समूल रूप से नष्ट कर दिया गया कारण कि वे सम्राट महापद्मनन्द के गौरवशाली इतिहास एवं उनके कुलवंश परम्परा को आगे किसी को भी बताना नहीं चाहते थे क्योंकि ये नापित राजन्यों (राजा के भाईयों) से जुड़कर पुरोहिती एवं यज्ञ अनुष्ठान का व्यवसाय चलाते थे जिससे नापित राजन्यों का गौरवमयी इतिहास बताना उनके लिए उचित नहीं था इसलिए ये केवल इन्हें अशिक्षा का ऐसा पाठ पठाये कि सेवा करना ही सर्वोपरि धर्म है जिससे यह राजवंश आगे चलकर सेवा करते-करते राजा से सेवक, प्रजा एवं गुलाम आदि बन गया। दूसरा कारण यह भी रहा कि लोग धीरे-धीरे नन्द राजवंश के गौरवशाली इतिहास को भूलते गये। तब तक ब्राहमण शिक्षा का मुख्य अधिकारी बन चुका था जिससे बहुसंख्यक मूलनिवासी समाज अशिक्षित होकर राजा से प्रजा के श्रेणी में आ गया।
नि:संकोच यहाँ कहना आवश्यक है कि यदि अंग्रेज भारत में शासन करने नहीं आये होते तो यहाँ कि आम जनता आज भी मुगलों एवं मुगलों के पूर्व के अन्धकार युग में स्थिति होती। अंग्रेजों को जब यहाँ शासन करना हुआ तो सबसे पहले यहाँ के प्राचीन साहित्यों, जैन, बौद्ध ग्रन्थों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों मनुस्मृति, रामायण एवं महाभारत आदि का अंग्रेजी में अनुवाद कराया और जानना चाहा कि यहाँ की प्राचीन इतिहास क्या है? यहाँ के लोग किन विचारों को आत्मसात् करके जीवन का निर्वहन करते है इत्यिादि को जानने में ही यहाँ का प्राचीन भारतीय इतिहास उजागर हो गया। अंग्रेजों ने सबको पढ़ने-लिखने का अवसर दिया। जिससे यहाँ का बहुसंख्यक अशिक्षित समाज शिक्षित अपने होकर आपको पहचाननें लगा, अपने इतिहास को जान सका अन्यथा आज भी ये लोग कुए के मेढ़क की तरह अज्ञानता में पड़े रहते।
तिब्बती लेखक तारानाथ ने बौद्विष्ठों पर किये गये अत्याचार का वर्णन किया है। इन्होंने लिखा है कि बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने घोषणा किया था कि जो कोई भी बौद्ध भिक्षुओं का सिर काटकर मुझे देगा उसे मैं सोने का सिक्का दूँगा। जिससे नापित बौद्ध शासकों एवं बौद्ध भिक्षुओं का काफी ह्वास हुआ।
जिस प्रकार मूल निवासी नन्द मौर्य राजवंश को एवं बौद्धिष्ठों को षड़यन्त्रों द्वारा इतिहास से मिटाया एवं हटाया गया उससे प्रतीत होता है कि उनसे सम्बन्धित लेखों पर भी खूब लीपा-पोती की गई है। उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हो गया है कि नाग, नन्द, मौर्य एवं गुप्त एवं गुप्त वंश एक ही रक्त एवं वंश परम्परा के शासक थे जिन्हें नाम या नामान्त के कारण भिन्न-भिन्न राजवंश का नाम देकर इतिहास में बताया गया है तथा इनके उत्पत्ति को अज्ञात बताकर एक ही अभिन्न राजवंश को भिन्न-भिन्न बताने का प्रयास किया गया है। जबकि ये सभी एक ही रक्त की सन्तान थे।
आचार्य शुभनारायण यथार्थी
मो.: ९५१७४६८४९२